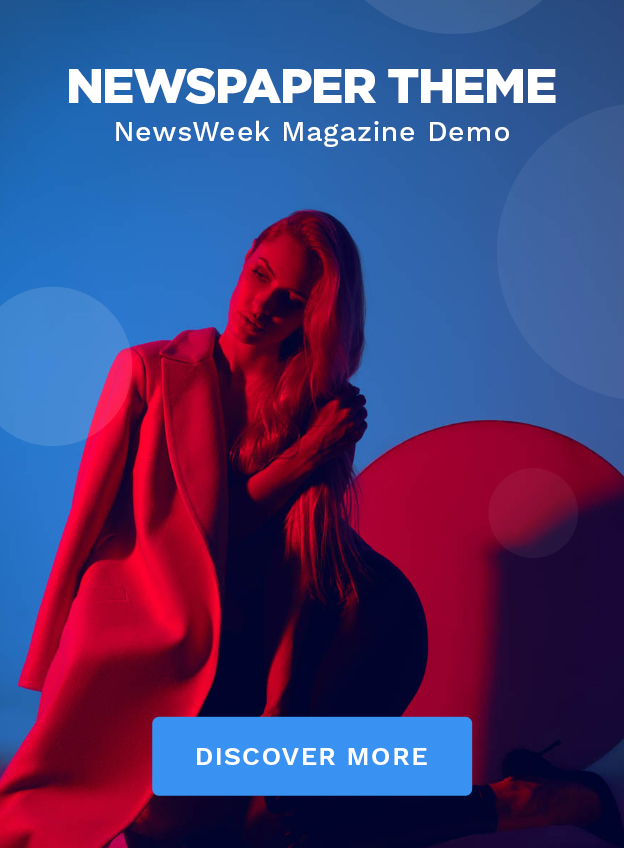(रईस खान)
हुज़ूर, आज का सुप्रीम कोर्ट का मंज़र तो किसी कड़क मुन्सिफ़ की तरह था, जिसने चुनाव आयोग को तलब करके पूछा, “जनाब, ये 65 लाख नाम आपने मतदाता सूची से ऐसे कैसे ग़ायब कर दिए? और वजह तक बताने की ज़हमत नहीं उठाई?” अदालत का लहजा महज़ कानूनी नहीं, बल्कि कुछ यूँ था जैसे मकान-मालिक किराएदार से कह दे, “भाई, किराया तो छोड़ो, हिसाब-किताब भी दबा रखोगे?”
असल सवाल यही है कि चुनाव आयोग आख़िर इतना अड़ियल रवैया क्यों अपनाए बैठा है? ये वही संस्था है, जिसके बारे में हमें बरसों से बताया जाता रहा कि वो ग़ैर-जानिबदार है, पारदर्शी है, और सिर्फ़ क़ानून की लकीर पर चलती है। मगर आज हालत ये है कि अदालत को खुद बीच में आना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का एतबार डगमगा रहा है। जब नाम हटाने की वजह तक ग़ायब हो, और मतदाता अपने ही हक़ के लिए दफ़्तर-दर-दफ़्तर ठोकरें खाए, तो क्या इसे ईमानदारी कहा जा सकता है?
अदालत का हुक्म साफ़ है—हर नाम और हटाने का सबब सार्वजनिक करो, ताकि अवाम को पता चले कि उनका नाम ग़ायब होने की वजह क्या है। मगर सोचिए, ये काम तो खुद आयोग का फ़र्ज़ था, अदालत का नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बुनियादी मसले पर दख़ल देना पड़ रहा है, तो या तो व्यवस्था में लापरवाही है, या नीयत में धुंधलापन। और दोनों ही हालत में नुक़सान लोकतंत्र का है।
ईमानदारी सिर्फ़ क़ानून की किताब में लिख देने से साबित नहीं होती, वो दिखनी भी चाहिए। अगर आयोग वाक़ई बेदाग़ है, तो उसे हर आंकड़ा, हर वजह, और हर प्रक्रिया को ऐसे पेश करना चाहिए जैसे सूरज अपनी रोशनी पेश करता है—बिना पर्दे के, बिना लाग-लपेट के। वरना, लोग यही समझेंगे कि मतदाता सूची का खेल कोई पारदर्शी अमल नहीं, बल्कि बंद कमरे में खेले जाने वाली वो बाज़ी है, जिसमें मोहरे हमेशा किसी के हक़ में गिरते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आईना दिखाया है, उसमें सिर्फ़ आयोग की सूरत नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चेहरा भी झलक रहा है। सवाल ये है—क्या आयोग इस आईने में खुद को देखकर शर्माएगा, या फिर पुराने रटे-रटाए जुमलों से उसे ढकने की कोशिश करेगा? क्योंकि जनाब, अवाम के सब्र का प्याला भी हमेशा भरता नहीं—कभी न कभी छलक ही जाता है।