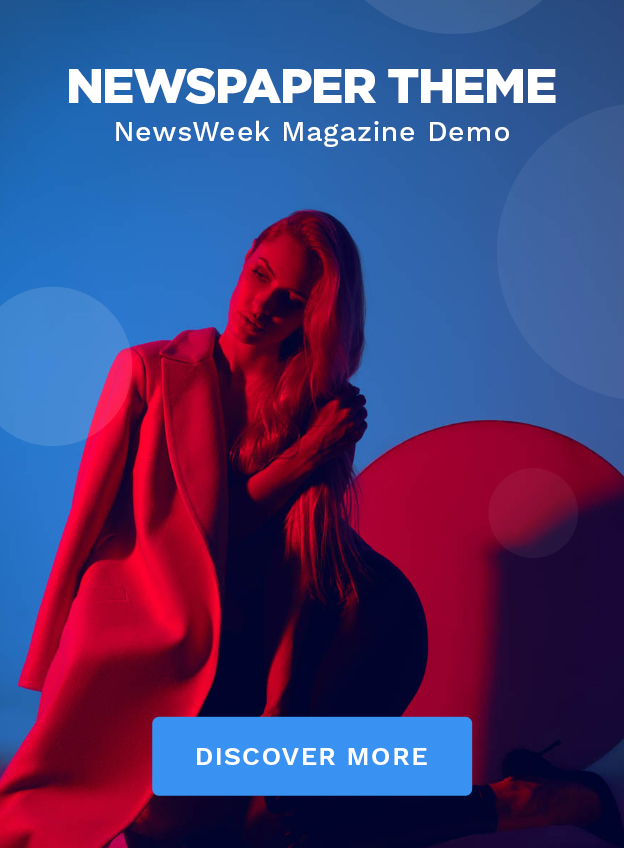(रईस खान)
बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद भड़की हिंसा और मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। “आई लव मोहम्मद” अभियान के समर्थन में भीड़ जमा हुई, पत्थरबाज़ी हुई, पुलिसकर्मी घायल हुए और अंततः मौलाना को हिरासत में भेज दिया गया। अब बहस यह है कि क्या यह कदम कानून की मजबूरी थी या राजनीति की चाल?
मज़हबी सिलसिला और राजनीतिक खेल
तौकीर रज़ा कोई मामूली नाम नहीं। बरेलवी मत के इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ की वंशावली से होने के कारण उन्हें मज़हबी असर हासिल है। यही वजह है कि उनके इशारे पर हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। कभी कांग्रेस तो कभी समाजवादी पार्टी, हर दौर में उन्होंने सियासी तालमेल साधकर अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन उनकी पहचान ज़्यादा तर भीड़ और विवादों से ही जुड़ी रही है।
भीड़ से रहनुमाई तक, अधूरा सफ़र
यह पहली बार नहीं कि उनके नाम पर हिंसा का धब्बा लगा हो। 2010 के बरेली दंगे हों या हालिया बवाल, हर जगह सवाल यही रहा, क्या मौलाना सिर्फ़ भीड़ जुटाना जानते हैं या उन्हें काबू में रखना भी आता है? उनका दावा है कि प्रशासन ने उन्हें नज़रबंद कर आवाज़ दबाई, जबकि पुलिस का आरोप है कि पूरी योजना पहले से तय थी।
समर्थक बनाम आलोचक
समर्थकों की नज़र में मौलाना मज़हबी अस्मिता की आवाज़ हैं। मगर आलोचक उन्हें साम्प्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताते हैं। कभी आरएसएस और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कहकर विवाद खड़ा किया, कभी वोटों को मज़हब के नाम पर बाँटने की बात की। नतीजा यह कि उनका नाम हमेशा किसी न किसी टकराव से जुड़ा रहा।
बरेली की यह गिरफ्तारी सिर्फ़ एक घटना नहीं, बल्कि आईना है। रहनुमाई का असली मक़सद भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि उसे सही मंज़िल तक ले जाना है। नारे और टकराव तालीम और तरक़्क़ी का विकल्प नहीं हो सकते। सवाल यह है कि मौलाना तौकीर रज़ा जैसे नेता कब समझेंगे कि समाज को जज़्बाती नारों से नहीं, बल्कि अमली तरक़्क़ी से नया मक़ाम मिलेगा?