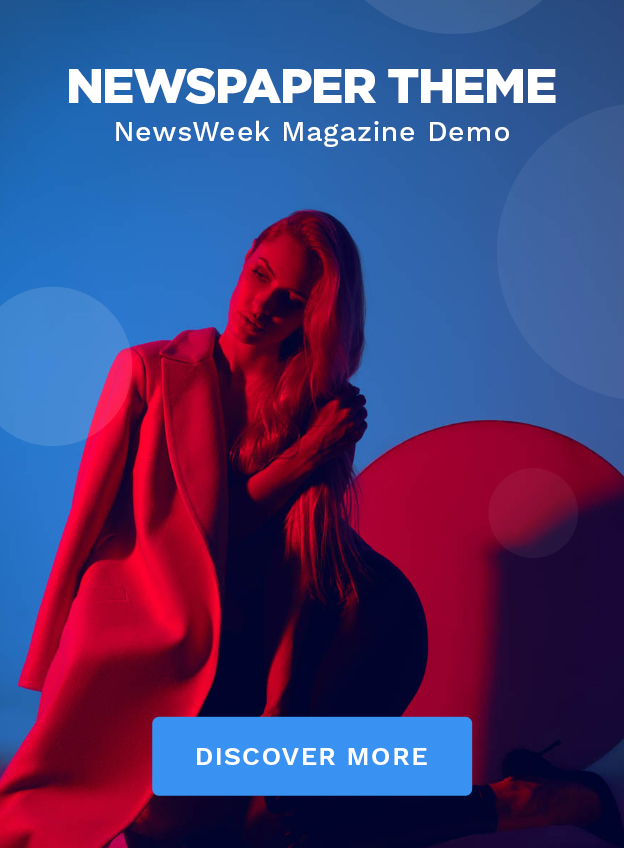ज़हरा निगाह की तालीम हैदराबाद दकन और कराची में हुई। यह घर के अदबी माहौल का ही असर था कि ज़हरा निगाह महज़ ग्यारह बरस की उम्र से ही शायरी करने लगी थीं। बीसवीं सदी में जिन ख़वातीन ने अपनी शायरी के ज़रिए नसाई जज़्बात की तरजुमानी की, उनमें दो नाम क़ाबिले-ज़िक्र हैं, पहला अदा जाफ़री का और दूसरा ज़हरा निगाह का। इन दोनों ने उस वक़्त शायरी शुरू की जब औरतों का कुछ लिखना ठीक नहीं समझा जाता था। यह वह दौर था जब किसी शायरा का कलाम रिसाला ‘नक़ूश’ में छपता था तो शायरा के नाम के साथ ब्रेकेट में ‘तवायफ़’ लिखा जाता था। इन हालात में किसी लड़की का शायरी करना और अपनी शायरी को कहीं छपवाना दिल-गुर्दे का काम था।
ज़हरा निगाह को शेर-ओ-अदब का माहौल बचपन से ही मयस्सर आया। उनके वालिदैन आला अदबी ज़ौक़ रखते थे। यही वजह है कि इस घर में परवरिश पाने वालों ने अदब, सहाफ़त, ड्रामा निगारी और स्क्रिप्ट राइटिंग के मैदान में नमूदार मक़ाम हासिल किया। ज़हरा निगाह की अदबी ख़िदमात का तफ़्सील से ज़िक्र करने से पहले उनके ख़ानदानी पस-ए-मंज़र का मालूम होना ज़रूरी है।
ज़हरा निगाह का असल नाम फ़ातिमा ज़हरा और क़लमी नाम ज़हरा निगाह है। उनकी विलादत 14 मई 1937 को हिन्दुस्तान के हैदराबाद दकन में हुई। उनके वालिद क़मर मक़सूद बदायूं से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद दकन को अपना ठिकाना बना लिया था। बंटवारे के बाद यह ख़ानदान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के शहर कराची में आबाद हो गया। ज़हरा निगाह की तालीम हैदराबाद दकन और कराची में हुई। यह घर के अदबी माहौल का ही असर था कि वह महज़ ग्यारह बरस की उम्र से ही शायरी करने लगी थीं। उन्होंने अपनी पहली नज़्म ‘गुड़िया गुड्डे की शादी’ लिखी थी, जिसे पढ़कर उनकी टीचर ने उन्हें बाक़ायदा शायरी करने और मुशायरों में शिरकत का मशवरा दिया था।
शुरुआत में ज़हरा ने अपना कलाम वालिद को दिखाया जो उनकी हौसला-अफ़ज़ाई करते थे। पंद्रह बरस की उम्र में ही ज़हरा निगाह ने अपनी ख़ूबसूरत आवाज़ और अंदाज़ की वजह से मुशायरों में धूम मचाना शुरू कर दिया था। कम-उम्र में उनकी पुख़्ता कलामी को देखकर लोगों को गुमान होने लगा कि वह किसी बड़े शायर का कलाम पढ़ती हैं। लेकिन कुछ ही अर्से में यह ग़लतफ़हमी दूर हो गई। ज़हरा निगाह ने जिगर मुरादाबादी से अपने कलाम पर इस्लाह लेने की कोशिश की थी, लेकिन जिगर साहब ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि, “तुम्हारा ज़ौक़ ख़ुद ही तुम्हारे कलाम की इस्लाह कर देगा।”
ज़हरा निगाह जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, उसके बारे में यह कहा जाए कि “ईं ख़ाना तमाम आफ़ताब अस्त” तो ग़लत नहीं होगा। मशहूर ड्रामा-निगार फ़ातिमा सुरैया, मशहूर ब्रॉडकास्टर और मुहक़्क़िक़ा सारा नक़वी उनकी बहनें थीं। एक बहन ज़ुबैदा तारिक़ पाकिस्तान की पहली मशहूर कुक थीं जिनके शोज़ टेलीविज़न पर आते थे। मशहूर मज़ाह निगार, स्क्रिप्ट राइटर, टी.वी. मेज़बान और मुसव्विर अनवर मक़सूद उनके भाई हैं। एक भाई अहमद मक़सूद आला सरकारी ओहदेदार रहे।
ज़हरा निगाह ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को मख़्फ़ी रखा है, इसलिए उनकी शख़्सियत और हालात-ए-ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात आम नहीं हैं। हालाँकि उन्होंने बायोग्राफी तहरीर की है लेकिन उसे शाया नहीं किया। उनका कहना है कि “यह ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जो मैंने अपने बच्चों के लिए क़लम-बंद किए हैं, और वे इसे पढ़ने के बाद नज़र-ए-आतिश कर देंगे।”
ज़हरा ने अपनी शायरी का आग़ाज़ ग़ज़ल से किया था, मगर बाद में नज़्म की तरफ़ माइल हो गईं और नज़्म-गोई में अपना ख़ास मक़ाम बनाया। उनकी कई नज़्में बहुत मक़बूल हुईं। उनकी नज़्म-गोई का क़सीदा फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जैसे शायर ने पढ़ा है। फ़ैज़ कहते हैं, “उनकी मंज़ूमात में न तो जदीदियत के ग़ैर-शायराना जज़्बात का कोई बनावट है और न रुमानियत की शायराना आराइश-पसंदी का कोई दख़ल है। रवायती नक़्श-ओ-निगार और आराइश रंग-ओ-रोगन का सहारा लिए बग़ैर दिल लगने वाला शेर कहना बहुत दिल-गुर्दे का काम है।”
औरत के जज़्बात की तरजुमानी ज़हरा निगाह की शायरी की इम्तियाज़ी ख़ासियत है। उनकी अक्सर नज़्मों का मौजूं औरत, उसकी हस्सियत, उसकी ज़ेहनी उलझनें और उसके मसाइल हैं। ज़हरा निगाह के यहाँ रवायती मशरिक़ी औरत के मुख़्तलिफ़ रंग-ओ-रूप मौजूद हैं।
भरा घर मेरा इक खाली मकां है
कहीं कुछ है तो एहसास-ए-ज़ियां है
यह सच है यहाँ शोर ज़्यादा नहीं होता
घर-बार के बाज़ार में पर क्या नहीं होता
हर जज़्बा-ए-मासूम की लग जाती है बोली
कहने को ख़रीदार पराया नहीं होता
औरत के ख़ुदा दो हैं हक़ीक़ी व मिज़ाज़ी
पर उसके लिए कोई भी अच्छा नहीं होता
मैं बच गई माँ उनकी ऐसी नज़्म है जो एक औरत ही लिख सकती है:
मैं बच गई माँ
मैं बच गई माँ
तेरे कच्चे लहू की मेंहदी
मेरे पूर-पूर में रच गई माँ
मैं बच गई माँ
गर मेरे नक़्श उभर आते
वो फिर भी लहू से भर जाते
मेरी आँखें रोशन हो जातीं तो
तेज़ाब का सुरमा लग जाता
सट्टे-वट्टे में बंट जाती
बेकारी में काम आ जाती
हर ख़्वाब अधूरा रह जाता
मेरा क़द जो थोड़ा-सा बढ़ता
मेरे बाप का क़द छोटा पड़ता
मेरी चुनरी सर से ढलक जाती
मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती
तेरी लोरी सुनने से पहले
अपनी नींद में सो गई माँ
अंजान नगर से आई थी
अंजान नगर में खो गई माँ
मैं बच गई माँ
मैं बच गई माँ
ज़हरा निगाह ने घर के सीमित आंगन से लेकर अंतरराष्ट्रीय हदूद तक बहुत से मौज़ूआत पर लिखा। मुआशरे की अफ़रातफ़री, लाक़ानूनियत, ज़ुल्म-ओ-बरबरियत के दरम्यान इंसान की बेचारगी पर भी उन्होंने क़लम उठाया। अफ़रातफ़री के माहौल में इंसान का अरसा-ए-हयात तंग होता देखकर उन्होंने “सुना है” के उन्आन से एक ऐसी नज़्म कही जिसे उनकी शाहकार नज़्म कहा जा सकता है।
सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है
सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता
दरख़्तों की घनी छाँव में जाकर लेट जाता है
हवा के तेज़ झोंके जब दरख़्तों को हिलाते हैं
तो मैना अपने बच्चे छोड़कर
कौए के अंडों को परों से थाम लेती है
सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है
सुना है जब किसी नदी के पानी में
बये के घोंसले का गंदमी रंग लरज़ता है
तो नदी की रूपहली मछलियाँ उसको पड़ोसन मान लेती हैं
कभी तूफ़ान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो
किसी लकड़ी के तख़्ते पर गिलहरी, साँप, बकरी और चीता साथ होते हैं
सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है
ख़ुदावंदा! जलील-ओ-मोतबर! दाना-ओ-बेना! मुनसिफ़-ओ-अकबर!
मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई क़ानून नाफ़िज़ कर।
ज़हरा निगाह की नज़्म “समझौता” में एक ऐसी औरत नज़र आती है जो मुआशरे के इस्तेहसाल के दौरान कदम-कदम पर समझौते करती हुई ज़िंदगी से निबाह किए जा रही है।
मुलायम गर्म समझौते की चादर
यह चादर मैंने बरसों में बुनी है
कहीं भी सच के गुल-बूटे नहीं हैं
किसी भी झूठ का टांका नहीं है
इसी से मैं भी तन ढक लूँगी अपना
इसी से तुम भी आसूदा रहोगे
न खुश होगे न पज़मर्दा रहोगे
इसी को तानकर बन जाएगा घर
बिछा लेंगे तो खिल उठेगा आँगन
उठा लेंगे तो गिर जाएगी चिलमन
ज़हरा निगाह की ग़ज़लों का आहंग भी दीगर शायरात से जुदा है। लेकिन इस आहंग से भी औरत के जज़्बात व एहसासात हम-आहंग नज़र आते हैं। उनकी ग़ज़लों में निजी जज़्बात व एहसासात भी हैं, इज्तिमाई मसाएब का बयान भी और इश्क़ की वारदात भी। औरत की बेबसी भी है और घुटन की लहर भी, लेकिन उन्होंने अपने लहजे की इनफ़िरादियत को कभी क़ुर्बान नहीं किया।
शब भर का तेरा जागना अच्छा नहीं ज़हरा
फिर दिन का कोई काम भी पूरा नहीं होता
बड़े सुकून से काटा अज़ाब-ए-तनहाई
मैं अपने आप से मुद्दत के बाद मिल पाई
ख़ताएँ दोनों की एक-सी थीं पर तअज्जुब है
किसी को दाद मिली और किसी को रुस्वाई
कभी एक लफ़्ज़ के सौ-सौ मआनी
कभी सारी कहानी अनकही थी
हँसती-बस्तियों राहों का ख़ुश-बाश मुसाफ़िर
रोज़ी की भट्टी का ईंधन बन जाता है
दफ़्तर, मन्सब , दोनों ज़ेहन को खा लेते हैं
घर वालों की क़िस्मत में तन रह जाता है
देखते-देखते एक घर के रहने वाले
अपने-अपने ख़ानों में बँट जाते हैं
इतनी बड़ी शायरा होने के बावजूद ज़हरा निगाह ने बहुत कम लिखा, लेकिन जितना भी लिखा क़ीमती लिखा और उसे बहुत सराहा गया। उनके कलाम के जो मजमूआत शाया हुए वो हैं , “शाम का पहला तारा”, “वक़्त” और “फ़िराक़”। “लफ़्ज़ लफ़्ज़” के उनआन से उनकी कुल्लियात भी शाया हुई है। वे अभी बाक़ैद-ए-हयात हैं और क़लमी व फ़िक्री तौर पर सरगर्म हैं।