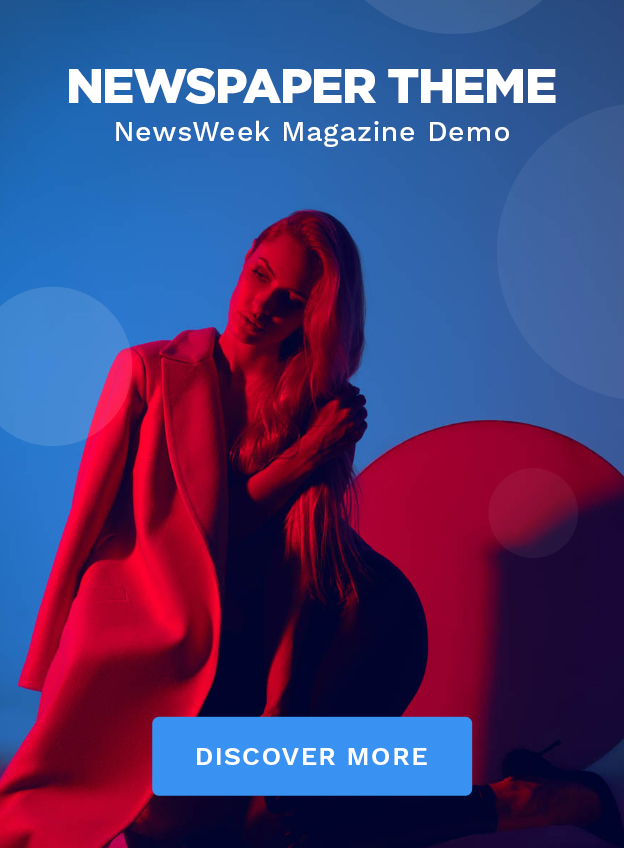(रईस खान)
“क़ौम की तरक़्क़ी तालीम से होती है और तालीम की कमी ही पस्ती का सबब है।” हिंदुस्तानी मुसलमानों की मौजूदा हालत इसी हक़ीक़त की गवाही देती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सबसे पिछड़े तबक़े की फ़ेहरिस्त में मुसलमानों का नाम शामिल है। वजह सिर्फ़ एक नहीं, सरकारी नीतियाँ भी और समाज की अपनी कोताहियाँ भी।
आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने IIT, UGC और साहित्य अकादमी जैसी बुनियादें रखीं। उनका ख़्वाब था कि हर बच्चा पढ़े और मुसलमान तालीम के ज़रिए पिछड़ेपन से बाहर निकले। मौलाना हसरत मोहानी और अहमद किदवई जैसे लीडरों ने भी तालीम को क़ौमी तरक़्क़ी का असली ज़रिया माना। लेकिन सरकारों ने इन कोशिशों को वह तवज्जो कभी नहीं दी जिसकी दरकार थी। मुस्लिम इलाक़ों में स्कूल और कॉलेज की जगह वादों और नारों ने जगह ली।
सच्चर कमेटी रिपोर्ट (2006) ने साफ़ लिखा था कि मुसलमानों की साक्षरता दर उस वक़्त सिर्फ़ 59% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 65% से ऊपर था। उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी 4% से भी कम थी। यहाँ तक कि शहरी इलाक़ों में भी 25% मुस्लिम बच्चे मिडिल स्कूल तक पहुँचने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते थे। आज भी कई सरकारी रिपोर्टें दिखाती हैं कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
जहाँ मुसलमानों ने अपने दम पर तालीमी इदारे खड़े किए, वहाँ भी रुकावटें खड़ी की गईं। आज़म ख़ान की जौहर यूनिवर्सिटी ने हज़ारों ग़रीब और मज़लूम बच्चों को तालीम देने का काम शुरू किया। लेकिन इसके खिलाफ़ एक के बाद एक मुक़दमें, ज़मीन की ज़ब्ती और प्रशासनिक छापे इस क़दर बढ़े कि यूनिवर्सिटी को ताला लगाने तक की नौबत आई। यही हाल सहारनपुर के हाजी मो. इक़बाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी का हुआ, जिसे मुसलमानों के लिए एक बड़े तालीमी सेंटर के तौर पर बसाया गया था। लेकिन हाजी इक़बाल के ख़िलाफ़ लगातार एंफ़ोर्समेंट और प्रशासनिक कार्रवाइयों ने यूनिवर्सिटी को तंगदस्ती और बंदिशों के हालात में धकेल दिया। नतीजा यह निकला कि तालीम की जगह मुक़दमेबाज़ी और ताले ही बाकी रह गए।
अब सवाल यह है कि मुसलमान अपनी आने वाली नस्लों की तालीम का रास्ता किसके भरोसे तय करेंगे, सरकार पर, जिसने आज तक भरोसा तोड़ा है, या अपने दम पर, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने दिखाया है? जवाब साफ़ है: तालीम की जंग किसी और के सहारे नहीं जीती जाएगी। समाज को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, छोटे-छोटे स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों से लेकर बड़े तालीमी इदारों तक अपने दम पर क़दम बढ़ाने होंगे।
तालीमी इदारे सिर्फ़ इमारतें नहीं होते, बल्कि क़ौम की सोच और इरादे का आईना होते हैं। अगर मुसलमान वाक़ई अपनी नस्लों का मुक़द्दर बदलना चाहते हैं तो उन्हें समझना होगा कि यह लड़ाई सिर्फ़ तालीम से जीती जा सकती है, और यह लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी और जीतनी होगी।