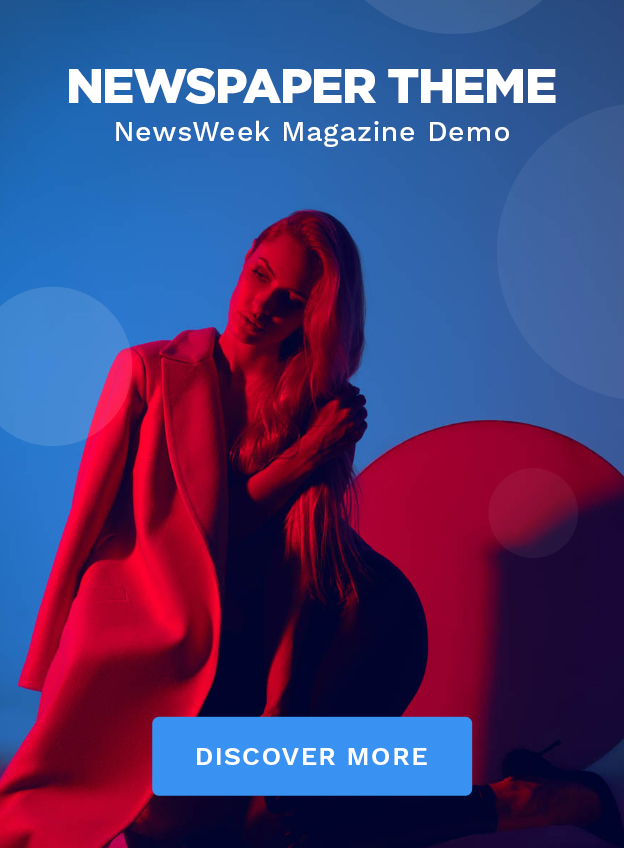(रईस खान)
बरेली में जुमे की नमाज़ के बाद जो कुछ हुआ, वह कोई नया वाक़िया नहीं। मौलाना तौकीर रज़ा के आह्वान पर भारी भीड़ जमा हुई, नारेबाज़ी हुई, पुलिस से टकराव हुआ और हालात बिगड़ गए। आख़िरी वक़्त में प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी तो ग़ुस्सा भड़क उठा। लेकिन असल सवाल यह है कि हर बार नमाज़ के बाद सियासी नारों की गूंज और फिर पुलिस-मुक़ाबले का नज़ारा क्यों दोहराया जाता है?
क़ौमी रहनुमाई या भीड़ की सियासत?
मज़हबी और सियासी रहनुमा भीड़ जुटाने में माहिर हैं। लेकिन जब वही भीड़ हाथ से निकल जाती है, तो वही रहनुमा ग़ायब हो जाते हैं। नतीजा हमेशा एक जैसा होता है, लाठीचार्ज, गिरफ़्तारियाँ, मुक़दमे और समाज की बदनामी। और इस सबकी क़ीमत चुकाता है आम मुसलमान, जिसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले ही मुश्किलों में घिरी हुई है।
आज़ादी के बाद से अब तक के दंगे और फ़सादात गवाह हैं कि सबसे ज़्यादा नुक़सान मुस्लिम समाज का हुआ है। जॉनसन आयोग की रिपोर्ट से लेकर मुंबई, मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर और गुजरात जैसे बड़े फ़सादात तक, हर जगह क़ब्रिस्तान की मिट्टी और घायल ज़िंदगियों की गवाही यही कहती है कि नुक़सान सिर्फ़ क़ौम का हुआ।
तालीम और तरक़्क़ी- क्यों ग़ायब अजेंडा?
सवाल उठता है कि क्यों यही मौलाना और सियासी रहनुमा कभी शिक्षा सुधार, बेरोज़गारी के ख़ात्मे या कारोबार की मज़बूती के लिए इस तरह का जुनून नहीं दिखाते? क्यों कभी लाखों की भीड़ “हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दो” या “हमारे नौजवानों को रोज़गार दो” के नारों के साथ सड़कों पर नहीं उतरी?
क्योंकि वहाँ मेहनत चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए और लम्बी जद्दोजहद चाहिए। भीड़ को भड़काना आसान है, मगर समाज की तालीम और तरक़्क़ी के लिए सालों काम करना मुश्किल। यही वजह है कि रहनुमाई के नाम पर हमें सिर्फ़ नारों और तात्कालिक सियासी लोकप्रियता का दिखावा मिलता है।
तारीख़ी मिसालें-राह कहाँ थी और कहाँ चली गई
अगर हम अपनी तारीख़ देखें, तो सर सैयद अहमद ख़ाँ का अलीगढ़ आंदोलन साफ़ दिखाता है कि असली रहनुमाई क्या होती है। उन्होंने तालीम को हथियार बनाया और पूरी क़ौम की सोच बदल दी। अल्लामा इक़बाल से लेकर मौलाना आज़ाद तक, हर बड़ी शख़्सियत ने यही कहा कि तरक़्क़ी का रास्ता तालीम और इल्म से होकर जाता है, न कि भीड़ और फ़साद से।
आज वही सवाल दुबारा खड़ा है। हमारी क़ौम का वक़्त और तवानाई नारेबाज़ी और टकराव में ज़ाया हो रहा है। अगर यही ताक़त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कारोबारी इदारों में लगाई जाए, तो क़ौम का नक़्शा बदल सकता है।
असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है
हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी पिछड़ने और नुक़सान की वजह बाहर है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा नुक़सान हमें भीतर बैठा रहनुमा पहुँचा रहा है। वह रहनुमा, जो भीड़ को ग़ुस्से में झोंक देता है, लेकिन तालीम और रोज़गार की जद्दोजहद में कभी साथ नहीं देता।
अब वक़्त है कि क़ौम अपने रहनुमाओं से सीधा सवाल करे:
“मौलाना साहब, हमारे बच्चों की तालीम के लिए आपकी क्या तदबीर है? हमारे नौजवानों की बेरोज़गारी का हल आपके पास क्या है? हमारे कारोबार को मज़बूत करने के लिए आपका नक़्शा-ए-अमल कहाँ है?”
रास्ता बदलना होगा
क़ौम को यह समझना होगा कि नारों और भीड़ों से कभी तरक़्क़ी नहीं होती। तरक़्क़ी तालीम, मेहनत, रोज़गार और कारोबार से होती है। अगर हमारे रहनुमा इस राह पर नहीं चलते, तो क़ौम को अपनी राह ख़ुद तय करनी होगी।
अब वक़्त आ गया है कि हम “फ़साद की सियासत” को ठुकराकर “तरक़्क़ी की जद्दोजहद” को अपनाएँ। वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी।