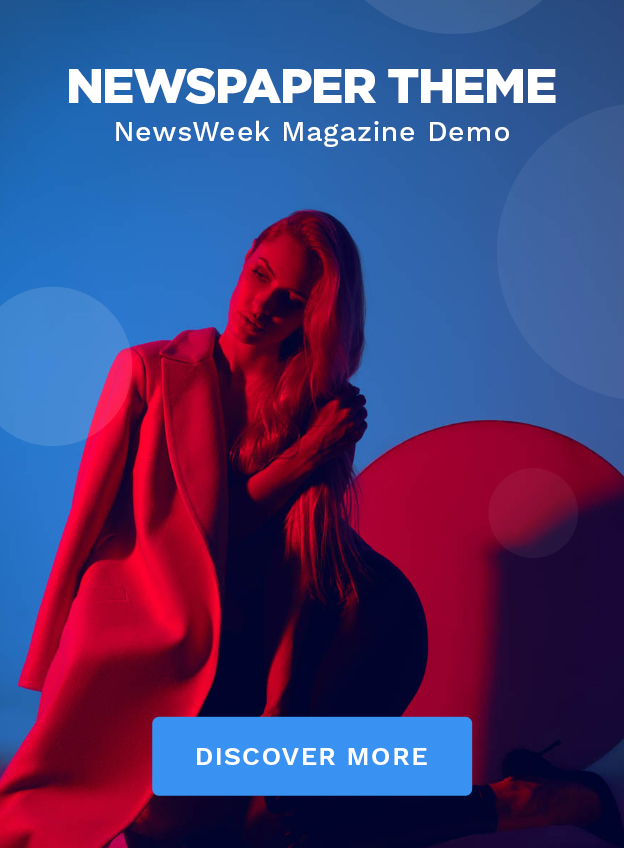(रईस खान)
देश में जब भी किसी विस्फोट या आतंकी घटना की खबर आती है, तो अक्सर मीडिया और जांच एजेंसियों का ध्यान कुछ विशेष नामों या पहचान वाले लोगों की ओर जल्दी चला जाता है। हाल ही दिल्ली में हुई विस्फोट की घटना के बाद जिस तरह कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया, उसने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हमारे देश में नाम और धर्म जांच से पहले ही अपराध तय कर देते हैं?
दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब किसी पढ़े-लिखे, पेशेवर मुस्लिम युवक या डॉक्टर को बिना ठोस सबूत के शक के घेरे में लाया गया हो। पिछले दो दशकों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ डॉक्टरों, इंजीनियरों या छात्रों को आतंकवाद से जुड़ा बताकर गिरफ्तार किया गया, लेकिन वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद वे निर्दोष साबित हुए। इन घटनाओं ने यह अहसास गहराया कि देश के भीतर एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ शिक्षा और तरक्की हासिल करने वाला मुस्लिम भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता।
मिसाल के तौर पर फरवरी 2019 में, नासिक की एक विशेष टाडा अदालत ने 11 मुस्लिम पुरुषों को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया। इन व्यक्तियों में तीन डॉक्टर और एक इंजीनियर शामिल थे, जिन्होंने निर्दोष साबित होने के लिए 25 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में, अब्दुल वाहिद शेख, जो एक पीएचडी छात्र और शिक्षक थे, सहित 12 मुस्लिम पुरुषों को बाद में बरी कर दिया गया, हालांकि कुछ को पहले दोषी ठहराया गया था।
अहमदाबाद, हैदराबाद और इसी तरह के कई अन्य मामलों में, जैसे 2005 हैदराबाद सुसाइड ब्लास्ट्स केस, कुछ व्यक्तियों को जेल में वर्षों बिताने के बाद निर्दोष घोषित किया गया। कुछ मामलों में सिविल इंजीनियर आसिफ खान और सॉफ्टवेयर इंजीनियर याह्या कम्मुकुट्टी जैसे पेशेवरों को भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बरी कर दिया गया।
2007 रामपुर CRPF टेरर में नवंबर 2025 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 साल बाद सभी 5 मुस्लिम व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिसमें निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया।
ऐसे मामलों में मीडिया की भूमिका अक्सर पक्षपातपूर्ण रही है। अधिकांश चैनल या अखबार बिना जांच पूरी हुए ही किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराने की भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं। यही वजह है कि “मीडिया ट्रायल” का चलन एक खतरनाक सामाजिक प्रवृत्ति बन चुका है। जब किसी समुदाय को बार-बार इस तरह के मामलों में बिना सबूत के जोड़ा जाता है, तो उसकी पूरी पीढ़ी अविश्वास और भय के माहौल में जीने लगती है।
बटला हाउस एनकाउंटर की घटना भी याद रखने योग्य है। 2008 में दिल्ली के जामिया नगर में हुए इस एनकाउंटर के बाद कई युवकों को “आतंकी” बताया गया, लेकिन बाद में कई स्वतंत्र रिपोर्टों और नागरिक संगठनों ने पुलिस के दावों पर गंभीर सवाल उठाए। इस घटना का असर खास तौर पर शिक्षित मुस्लिम युवाओं पर पड़ा, जो अब भी महसूस करते हैं कि चाहे वे कितनी भी तरक्की कर लें, उन्हें संदेह की दृष्टि से ही देखा जाएगा।
कई मीडिया अनुसंधानों ने भी यह दिखाया है कि भारतीय समाचार माध्यमों में मुस्लिम समुदाय की छवि अधिकतर “खतरे” या “अपराध” के संदर्भ में गढ़ी जाती है। उनकी उपलब्धियों, सामाजिक योगदान या वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रगति को शायद ही कभी वह प्रमुखता मिलती है जो नकारात्मक खबरों को दी जाती है। इससे एक ऐसा मनोवैज्ञानिक माहौल बनता है जहाँ समाज का एक हिस्सा यह मानने लगता है कि मुस्लिम नाम अपने आप में संदेह का प्रतीक है।
इस तरह के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होता है कि समस्या केवल पुलिस की नहीं, बल्कि मीडिया और समाज की सोच में भी है। जब किसी समुदाय को बार-बार अपराध और कट्टरता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है, तो वह धारणा आम जनमानस में गहरी बैठ जाती है। नतीजतन, जो मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या वैज्ञानिक अपने मेहनत और शिक्षा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें भी सामाजिक संदेह का बोझ झेलना पड़ता है।
जरूरत इस बात की है कि जांच एजेंसियां और मीडिया दोनों अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। किसी भी आरोप को साबित करने से पहले उसका पूरा सत्यापन होना चाहिए और किसी व्यक्ति या समुदाय को उसकी पहचान के आधार पर दोषी ठहराने से बचना चाहिए। भारतीय समाज की असली ताकत उसकी विविधता और सहअस्तित्व में है। अगर हम अपने ही शिक्षित और मेहनती नागरिकों को शक की निगाह से देखेंगे, तो यह केवल किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे देश की हार होगी।